परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े-लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की।
वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिये बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी नेतृत्त्व किया।उन्होंने तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में भाग लिया।
वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये जिसमें दलित वर्गों (कम्युनल अवार्ड) हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया।
वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया।वर्ष 1942 में डॉ. अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है।

परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल पढ़े-लिखे व्यक्ति और संत कबीर के अनुयायी थे। बाबा साहेब अंबेडकर ने बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और आगे की पढ़ाई न्यूयॉर्क में कोलंबिया विश्वविद्यालय एवं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में की।
वर्ष 1924 में उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण हेतु एक संगठन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों की स्थिति को उजागर करने के लिये बहिष्कृत भारत समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने मार्च 1927 में महाड सत्याग्रह का भी नेतृत्त्व किया।उन्होंने तीनों गोलमेज़ सम्मेलनों में भाग लिया।
वर्ष 1932 में डॉ. अंबेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किये जिसमें दलित वर्गों (कम्युनल अवार्ड) हेतु अलग निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया।
वर्ष 1936 में उन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा हेतु इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया।वर्ष 1942 में डॉ. अंबेडकर को भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और वर्ष 1946 में बंगाल से संविधान सभा हेतु चुना गया। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में याद किया जाता है।
डॉ. अंबेडकर वर्ष 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर उन्होंने वर्ष 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
30 सितंबर 1956 को बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर ने "अनुसूचित जाति महासंघ" को बर्खास्त करके "रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया" की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले ही 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में प्रेसीडेंसी की बैठक हुई। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। 1957 में पार्टी के छह सदस्य दूसरी लोकसभा के लिए चुने गए।
चैत्य भूमि, मुंबई में डॉ. भीमराव अंबेडकर का स्मारक है। उन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचार एवं योगदान विशेष रूप से जाति-आधारित भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई तथा सामाजिक न्याय के लिये संघर्ष में भारत के वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भी प्रासंगिक बने हुए हैं।
एक समावेशी और समतावादी समाज का उनका दृष्टिकोण, जैसा कि भारतीय संविधान में निहित है, देश के भविष्य के विकास के लिये एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है।
इसके अतिरिक्त सशक्तीकरण के साधन के रूप में शिक्षा पर उनका ध्यान वर्तमान समय में विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारत एक वैश्विक नेता के रूप में अपनी पूरी क्षमता हासिल करना चाहता है।
डॉ. अंबेडकर की विरासत भारत की राष्ट्रीय पहचान का एक अभिन्न अंग है और उनके विचार भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे।
Republican Party Of India (A) U.P.
महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले (11 अप्रैल 1827- 28 नवम्बर 1890) एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ”ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।सितम्बर 1873 में इन्होने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतो के उत्थान के लिय इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे।
महात्मा ज्योतिबा फुले का मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। ज्योतिबा फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री-पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थीं। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं।
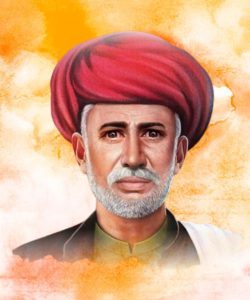 महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले (11 अप्रैल 1827- 28 नवम्बर 1890) एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ''ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।सितम्बर 1873 में इन्होने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतो के उत्थान के लिय इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे।
महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले (11 अप्रैल 1827- 28 नवम्बर 1890) एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रान्तिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ''ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।सितम्बर 1873 में इन्होने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। महिलाओं व पिछड़े और अछूतो के उत्थान के लिय इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गो को शिक्षा प्रदान करने के ये प्रबल समर्थक थे। वे भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे।
महात्मा ज्योतिबा फुले का मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। ज्योतिबा फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री-पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थीं। स्त्रियों की तत्कालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे इसीलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थीं।
महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 ई. में पुणे में हुआ था। एक वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन-पालन एक बायी ने किया। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था। इसलिए माली के काम में लगे ये लोग 'फुले' के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की सातवीं कक्षा की पढाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाजसेवी बनीं। दलित व स्त्रीशिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति-पत्नी ने मिलकर काम किया वह एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे।
उन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किया, इसके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफी प्रयास किये। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री फुले को इस योग्य बना दिया। कुछ लोगों ने आरम्भ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए।
ज्योतिबा को संत-महत्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में बड़ी रुचि थी। उन्हें ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने सब नर-नारी समान हैं तो उनमें ऊँच-नीच का भेद क्यों होना चाहिए। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया।
कुछ लोगों ने आरम्भ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किंतु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य, पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन विद्यालय खोल दिए।
निर्धन तथा निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 'सत्यशोधक समाज' 1873 मे स्थापित किया। उनकी समाजसेवा देखकर 1888 ई. में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हेंमहात्मा' की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण-पुरोहित के बिना ही विवाह-संस्कार आरम्भ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल-विवाह विरोधी और विधवा-विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं-गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत. महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने ‘एग्रीकल्चर एक्ट’ पास किया। धर्म, समाज और परम्पराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी।
Republican Party Of India (A) U.P.
भारत की प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक सावित्री बाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं।
महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवियत्री भी थीं उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में भी जाना जाता था।
सामाजिक मुश्किलें
वे स्कूल जाती थीं, तो विरोधी लोग उनपर पत्थर मारते थे। उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिये जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था तब ऐसा होता था।
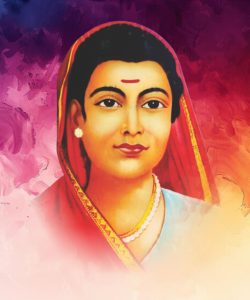 भारत की प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक सावित्री बाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं।
भारत की प्रथम महिला शिक्षक अध्यापक सावित्री बाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खन्दोजी नैवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1841 में ज्योतिराव फुले से हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं।
महात्मा ज्योतिराव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवियत्री भी थीं उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में भी जाना जाता था।
सामाजिक मुश्किलें
वे स्कूल जाती थीं, तो विरोधी लोग उनपर पत्थर मारते थे। उन पर गंदगी फेंक देते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिये जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था तब ऐसा होता था।
सावित्रीबाई पूरे देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिये उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थीं तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुँच कर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा बहुत अच्छे से देती हैं।
विद्यालय की स्थापना
5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्हों ने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले पाँच नये विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हे सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिये सन् 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ीं, बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त भी किया।
10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थीं। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण इनको भी छूत लग गया। और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई।
Republican Party Of India (A) U.P.
डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में वर्तमान-अम्बेडकर नगर जनपद नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। ढाई वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी (चन्दा देवी) का देहान्त हो गया।। उन्हें दादी के अलावा सरयूदेई, (परिवार की नाईन) ने पाला। टंडन पाठशाला में चौथी तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाईस्कूल में दाखिल हुए।
उनके पिताजी गाँधीजी के अनुयायी थे। जब वे गांधीजी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधीजी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए।
बंबई के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई की। लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली अगस्त को हड़ताल की। गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया। पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते सजा हुई। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई।
 डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में वर्तमान-अम्बेडकर नगर जनपद नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। ढाई वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी (चन्दा देवी) का देहान्त हो गया।। उन्हें दादी के अलावा सरयूदेई, (परिवार की नाईन) ने पाला। टंडन पाठशाला में चौथी तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाईस्कूल में दाखिल हुए।
डॉ. राममनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में वर्तमान-अम्बेडकर नगर जनपद नामक स्थान में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक व हृदय से सच्चे राष्ट्रभक्त थे। ढाई वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी (चन्दा देवी) का देहान्त हो गया।। उन्हें दादी के अलावा सरयूदेई, (परिवार की नाईन) ने पाला। टंडन पाठशाला में चौथी तक पढ़ाई करने के बाद विश्वेश्वरनाथ हाईस्कूल में दाखिल हुए।
उनके पिताजी गाँधीजी के अनुयायी थे। जब वे गांधीजी से मिलने जाते तो राम मनोहर को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इसके कारण गांधीजी के विराट व्यक्तित्व का उन पर गहरा असर हुआ। पिताजी के साथ 1918 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए।
बंबई के मारवाड़ी स्कूल में पढ़ाई की। लोकमान्य गंगाधर तिलक की मृत्यु के दिन विद्यालय के लड़कों के साथ 1920 में पहली अगस्त को हड़ताल की। गांधी जी की पुकार पर 10 वर्ष की आयु में स्कूल त्याग दिया। पिताजी को विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन के चलते सजा हुई। 1921 में फैजाबाद किसान आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। 1924 में प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के गया अधिवेशन में शामिल हुए। 1925 में मैट्रिक की परीक्षा दी। कक्षा में 61 प्रतिशत नंबर लाकर प्रथम आए। इंटर की दो वर्ष की पढ़ाई बनारस के काशी विश्वविद्यालय में हुई। कॉलेज के दिनों से ही खद्दर् पहनना शुरू कर दिया। 1926 में पिताजी के साथ गौहाटी कांग्रेस अधिवेशन में गए। 1927 में इंटर पास किया तथा आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता जाकर ताराचंद दत्त स्ट्रीट पर स्थित पोद्दार छात्र हॉस्टल में रहने लगे। विद्यासागर कॉलेज में दाखिला लिया। अखिल बंग विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में सुभाषचंद्र बोस के न पहुंचने पर उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1928 में कलकता में कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। 1928 से अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन में सक्रिय हुए। साइमन कमिशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया।कलकत्ता में युवकों के सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष तथा सुभाषचंद्र बोस और लोहिया विषय निर्वाचन समिति के सदस्य चुने गए। 1930 में द्वितीय श्रेणी में बीए की परीक्षा पास की।
1930 जुलाई को लोहिया अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वहाँ से वे बर्लिन गए। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो॰ बर्नर जेम्बार्ट को अपना प्राध्यापक चुना। 3 महीने में जर्मन भाषा सीखी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दाण्डी यात्रा प्रारंभ की। जब नमक कानून तोड़ा गया तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर पिता हीरालाल जी ने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा। 23 मार्च को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशन्स की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर सीटी बजाकर दर्शक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। सभागृह से उन्हें निकाल दिया गया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे बीकानेर के महाराजा द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर लोहिया ने रूमानिया की प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी बैठक में बंटवाई। गांधी इर्विन समझौते का लोहिया ने प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों की संस्था "मध्य यूरोप हिन्दुस्तानी संघ" की बैठक में संस्था के मंत्री के तौर पर समर्थन किया। कम्युनिस्टों ने विरोध किया। बर्लिन के स्पोटर्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुना। 1932 में लोहिया ने नमक सत्याग्रह विषय पर अपना शोध प्रबंध पूरा कर बर्लिन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
डॉ. लोहिया 1933 में मद्रास पहुंचे। रास्ते में सामान जब्त कर लिया गया। तब समुद्री जहाज से उतरकर हिन्दु अखबार के दफ्तर पहुंचकर दो लेख लिखकर 25 रुपया प्राप्त कर कलकत्ता गए। कलकत्ता से बनारस जाकर मालवीय जी से मुलाकात की। उन्होंने रामेश्वर दास बिड़ला से मुलाकात कराई जिन्होंने नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन दो हफ्ते साथ रहने के बाद लोहिया ने निजी सचिव बनने से इनकार कर दिया। तब पिता जी के मित्र सेठ जमुनालाल बजाज लोहिया को गांधी जी के पास ले गए तथा उनसे कहा कि ये लड़का राजनीति करना चाहता है।
कुछ दिन तक जमुनालाल बजाज के साथ रहने के बाद शादी का प्रस्ताव मिलने पर शहर छोड़कर वापस कलकत्ता चले गए। विश्व राजनीति के आगामी 10 वर्ष विषय पर ढाका विश्वविद्यालय में व्याख्यान देकर कलकत्ता आने-जाने की राशि जुटाई। पटना में 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में देश के समाजवादी अंजुमन-ए-इस्लामिया हॉल में इकट्ठे हुए, जहां समाजवादी पार्टी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यहां लोहिया ने समाजवादी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की। पार्टी के उद्देश्यों में लोहिया ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य जोड़ने का संशोधन पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। 21-22 अक्टूबर 1934 को बम्बई के बर्लि स्थित 'रेडिमनी टेरेस' में 150 समाजवादियों ने इकट्ठा होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य चुने गए। कांग्रेस सोशलिस्ट सप्ताहिक मुखपत्र के सम्पादक बनाए गए।
गांधी जी के विरोध में जाकर उन्होंने कांउसिल प्रवेश का विरोध किया। गांधी जी ने लोहिया के लेख पर दो पत्र लिखे। 1936 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के लिए पार्टी का दरवाजा खोल दिया। लोहिया बार-बार कम्युनिस्टों के प्रति सचेत रहने की चेतावनी जयप्रकाश नारायण जी एवं अन्य नेताओं को देते रहे। 1935 में जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहां लोहिया को परराष्ट्र विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया जिसके चलते उन्हें इलाहाबाद आना पड़ा। 1938 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में लोहिया राष्ट्रीय कार्यकारणी के सदस्य चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के परराष्ट्र विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस के कम्युनिस्टों को पार्टी से निकालने का निर्णय लिया गया। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस को समाजवादियों ने समर्थन किया। डॉ॰ लोहिया तटस्थ बने रहे। लोहिया ने गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर की बोस का चुनाव मेरी शिकस्त है पर प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव गांधी जी से सम्मानपूर्वक आह्वान करता है कि उनकी शिकस्त नहीं हुई है। गांधी जी की इच्छानुसार सुभाषचंद्र बोस कार्यसमिति बनाने को तैयार नहीं हुए तथा नेहरू सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं ने बोस के साथ कार्यसमिति में रहने से इंकार कर दिया तब बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया
Republican Party Of India (A) U.P.
राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, मराठा के भोंसले राजवंश के (26 जून, 1874 – 6 मई, 1922) राजा (शासनकाल 1894 – 1900) और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा (1900-1922) थे। उन्हें एक वास्तविक लोकतान्त्रिक और सामाजिक सुधारक माना जाता था। कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराजा, वह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य मणि था।
सामाजिक सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के योगदान से काफी प्रभावित, शाहू महाराज एक आदर्श नेता और सक्षम शासक थे जो अपने शासन के दौरान कई प्रगतिशील और पथ भ्रष्ट गतिविधियों से जुड़े थे। 1894 में अपने राजनेता से 1922 में उनकी मृत्यु तक, उन्होंने अपने राज्य में निचली जाति के विषयों के कारण अथक रूप से काम किया। जाति और पन्थ के बावजूद सभी को प्राथमिक शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी।
उनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल गाँव के घाटगे शाही मराठा परिवार में 26 जून, 1874 में जयश्रीराव और राधाबाई के रूप में यशवन्तराव घाटगे के रूप में हुआ था। जयसिंहराव घाटगे गाँव के प्रमुख थे, जबकि उनकी पत्नी राधाभाई मुधोल के शाही परिवार से सम्मानित थीं। नौजवान यशवन्तराव ने अपनी माँ को खो दिया जब वह केवल तीन थे।
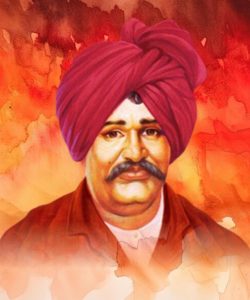 राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, मराठा के भोंसले राजवंश के (26 जून, 1874 - 6 मई, 1922) राजा (शासनकाल 1894 - 1900) और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा (1900-1922) थे। उन्हें एक वास्तविक लोकतान्त्रिक और सामाजिक सुधारक माना जाता था। कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराजा, वह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य मणि था।
राजर्षि छत्रपति शाहू जी महाराज, मराठा के भोंसले राजवंश के (26 जून, 1874 - 6 मई, 1922) राजा (शासनकाल 1894 - 1900) और कोल्हापुर की भारतीय रियासतों के महाराजा (1900-1922) थे। उन्हें एक वास्तविक लोकतान्त्रिक और सामाजिक सुधारक माना जाता था। कोल्हापुर की रियासत राज्य के पहले महाराजा, वह महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य मणि था।
सामाजिक सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के योगदान से काफी प्रभावित, शाहू महाराज एक आदर्श नेता और सक्षम शासक थे जो अपने शासन के दौरान कई प्रगतिशील और पथ भ्रष्ट गतिविधियों से जुड़े थे। 1894 में अपने राजनेता से 1922 में उनकी मृत्यु तक, उन्होंने अपने राज्य में निचली जाति के विषयों के कारण अथक रूप से काम किया। जाति और पन्थ के बावजूद सभी को प्राथमिक शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी।
उनका जन्म कोल्हापुर जिले के कागल गाँव के घाटगे शाही मराठा परिवार में 26 जून, 1874 में जयश्रीराव और राधाबाई के रूप में यशवन्तराव घाटगे के रूप में हुआ था। जयसिंहराव घाटगे गाँव के प्रमुख थे, जबकि उनकी पत्नी राधाभाई मुधोल के शाही परिवार से सम्मानित थीं। नौजवान यशवन्तराव ने अपनी माँ को खो दिया जब वह केवल तीन थे। 10 साल की उम्र तक उनकी शिक्षा उनके पिता द्वारा पर्यवेक्षित की गई थी। उस वर्ष, उन्हें कोल्हापुर की रियासत राज्य के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनन्दबीई ने अपनाया था। यद्यपि उस समय के गोद लेने के नियमों ने निर्धारित किया कि बच्चे को अपने नस में भोसले राजवंश का खून होना चाहिए, यशवन्तराव की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने एक अनोखा मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने राजकुमार कॉलेज, राजकोट में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेज़र से प्रशासनिक मामलों के सबक ले लिए। 1894 में उम्र के आने के बाद वह सिंहासन पर चढ़ गए, इससे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक राजसी परिषद ने राज्य मामलों का ख्याल रखा। अपने प्रवेश के दौरान यशवन्तराव का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज रखा गया था। छत्रपति शाहू ऊँचाई में पाँच फीट नौ इंच से अधिक था और एक शाही और राजसी उपस्थिति प्रदर्शित किया था। कुश्ती अपने पसन्दीदा खेलों में से एक थी और उन्होंने अपने पूरे शासन में इस खेल को संरक्षित किया था। पूरे देश के पहलवान कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अपने राज्य आएँगे।
1891 में बड़ौदा के एक महान व्यक्ति की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलाकर से उनका विवाह हुआ। इस जोड़े के चार बच्चे थे - दो बेटे और दो बेटियाँ।
जब शाही परिवार के ब्राह्मण पुजारी ने वैदिक भजनों के अनुसार गैर-ब्राह्मणों के संस्कार करने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने पुजारियों को हटाने और गैर-ब्राह्मणों के धार्मिक शिक्षक के रूप में एक युवा मराठा को नियुक्ति के लिए साहसी कदम उठाया क्षत्र जगद्गुरु (क्षत्रिय के विश्व शिक्षक) के। इसे वेदोकता विवाद के रूप में जाना जाता था। यह उसके कानों के बारे में एक सींग का घोंसला लाया, लेकिन वह विपक्ष के चेहरे पर अपने कदमों को पीछे हटाने वाला आदमी नहीं था। वह जल्द ही गैर-ब्राह्मण आन्दोलन के नेता बने और मराठों को उनके बैनर के तहत एकजुट कर दिया।
छत्रपति शाहू ने 1894 से 1922 तक 28 वर्षों तक कोल्हापुर के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की। शहू महाराज को निचली जातियों में से बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ करने का श्रेय दिया जाता है और वास्तव में यह मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने इस प्रकार शिक्षित छात्रों के लिए उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित किया, जिससे इतिहास में सबसे पुरानी सकारात्मक कार्रवाई (कमजोर वर्गों के लिए 50% आरक्षण) कार्यक्रमों में से एक बना। इन उपायों में से कई को 26 जुलाई को 1902 में प्रभावित किया गया था। उन्होंने रोजगार प्रदान करने के लिए 1906 में शाहू छत्रपति बुनाई और स्पिनिंग मिल शुरू की। राजाराम कॉलेज शाहू महाराज द्वारा बनाया गया था और बाद में इसका नाम उनके नाम पर रखा गया था। उनका जोर शिक्षा पर था और उनका उद्देश्य लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का था। उन्होंने अपने विषयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने विभिन्न जातियों और धर्मों जैसे पंचल, देवदान्य, नाभिक, शिंपी, धोर-चंभहर समुदायों के साथ-साथ मुसलमानों, जैनों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग छात्रावास स्थापित किए।
उन्होंने समुदाय के सामाजिक रूप से संगठित खंडों के लिए मिस क्लार्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियां पेश कीं। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए एक अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा भी शुरू की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की जिन्होंने सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को शास्त्रों को सीखने और संस्कृत शिक्षा को प्रचारित करने में सक्षम बनाया।
उन्होंने बेहतर प्रशासकों में उन्हें बनाने के लिए गांव के प्रमुखों या 'पैटिल' के लिए विशेष विद्यालय भी शुरू किए।
छत्रपति साहू समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक था और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया जब उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इंकार कर दिया। उन्होंने पद में एक युवा मराठा विद्वान नियुक्त किया और उन्हें 'क्षत्र जगद्गुरु' (क्षत्रिय के विश्व शिक्षक) का खिताब दिया। यह घटना शाहु के गैर-ब्राह्मणों को वेदों को पढ़ने और पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ महाराष्ट्र में वेदोकता विवाद का कारण बन गई। वेदोकता विवाद ने समाज के अभिजात वर्ग के विरोध से विरोध का तूफान लाया; छत्रपति के शासन का एक दुष्परिणाम। उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में दक्कन रायट एसोसिएशन की स्थापना की। एसोसिएशन ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। शाहुजी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे, और उन्होंने फुले द्वारा गठित सत्य शोधक समाज का संरक्षण किया। अपने बाद के जीवन में, हालांकि, वह आर्य समाज की तरफ चले गए।
Republican Party Of India (A) U.P.
© 2024. Republican Party Of India (A) U.P. All Rights Reserved.